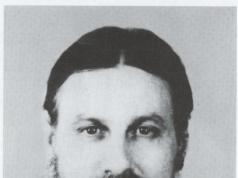(ग्रीक एटमॉस - भाप और स्पैरा - बॉल) - पृथ्वी का वायु कवच। वायुमंडल की कोई तीव्र ऊपरी सीमा नहीं है। इसके कुल द्रव्यमान का लगभग 99.5% निचले 80 किमी में केंद्रित है।
पर गैसों के निकलने के परिणामस्वरूप वातावरण उत्पन्न हुआ। इसका गठन बाद में महासागरों के उद्भव से प्रभावित हुआ और।
वातावरण की संरचना
कई मुख्य परतें हैं, जो विशेषताओं, घनत्व आदि में भिन्न हैं। निचली परत क्षोभमंडल है। यह पृथ्वी द्वारा गर्म होता है, जो बदले में सूर्य द्वारा गर्म होता है। क्षोभमंडल की सबसे गर्म परतें पृथ्वी से सटी हुई हैं। ऊंचाई के साथ ताप कम हो जाता है, और यह समुद्र तल पर +14°C से क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर -55°C तक गिर जाता है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि यहाँ का तापमान प्रत्येक 100 मीटर पर औसतन 0.6° गिर जाता है। इस मान को ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता कहा जाता है। क्षोभमंडल की मोटाई अलग है: यह 17 किमी है, और ध्रुवीय अक्षांशों के ऊपर यह 8-9 किमी है। केवल क्षोभमंडल में ही बादल बनना, वर्षा होना और अन्य घटनाएं होती हैं। क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल (50-55 किमी तक) है, जो एक संक्रमण परत - ट्रोपोपॉज़ द्वारा निचले हिस्से से अलग होता है। समताप मंडल में, हवा दुर्लभ अवस्था में है; यहाँ बादल नहीं बनते, क्योंकि व्यावहारिक रूप से कोई जल स्क्रीन नहीं है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी जारी रहती है, लेकिन 25 किमी से ऊपर प्रति किलोमीटर 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने लगती है। यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य के कारण होता है कि ओजोन परत सौर विकिरण को अवशोषित और बिखेरती है, जिससे इसे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोका जाता है। समताप मंडल के ऊपर एक संक्रमण क्षेत्र भी है - स्ट्रैटोपॉज़, जिसके बाद वायुमंडल की अगली परत आती है - मेसोस्फीयर (80-85 किमी तक)। यहां हवा और भी पतली है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। इससे भी ऊंची एक परत है जिसे थर्मोस्फीयर कहा जाता है। वायुमंडल की इन परतों (50 किमी से ऊपर) में जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाएं इसे विद्युत प्रवाहकीय बनाती हैं। चूँकि प्रतिक्रियाओं से आयन निकलते हैं, वायुमंडल का ऊपरी भाग, जिसमें मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर शामिल हैं, आयनोस्फीयर कहलाता है। इन परतों में ही क्या होता है। 800 किमी से ऊपर बहिर्मंडल ("एक्सो" - बाहरी) है, यहां गैस के कण बहुत दुर्लभ हैं, और तापमान +2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वायुमंडल की गैस संरचना का अध्ययन लंबे समय से किया गया है। 1774 में फ़्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवॉज़ियर ने वायु के मुख्य भागों का अध्ययन किया और वहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उपस्थिति स्थापित की। इसके बाद पता चला कि इन गैसों के अलावा हवा में अन्य गैसें भी हैं। इस प्रकार, वायु पृथ्वी की सतह पर निम्नलिखित घटकों से युक्त गैसों का मिश्रण है:
- नाइट्रोजन - 78%
- ऑक्सीजन - 21%
- अक्रिय गैसें - 0.94%
- कार्बन डाइऑक्साइड - 0.03%
- जल वाष्प और अशुद्धियाँ - 0.03%।
प्रकृति एवं मानव जीवन में वायुमण्डल का महत्व
- गैसीय आवरण के लिए धन्यवाद, पृथ्वी की सतह दिन के दौरान गर्म नहीं होती है और रात में उतनी ठंडी नहीं होती है, उदाहरण के लिए, वायुमंडल से रहित सतह;
- वायुमंडल पृथ्वी की रक्षा करता है, जिसका अधिकांश भाग जल जाता है और ग्रह की सतह तक नहीं पहुंचता है;
- ओजोन स्क्रीन () मानवता को अतिरिक्त पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, जिसकी एक बड़ी खुराक शरीर के लिए हानिकारक है;
- वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन सभी जीवित जीवों के सांस लेने के लिए आवश्यक है।
वातावरण का अध्ययन
मानवता लंबे समय से हवा के महासागर में रुचि रखती है, लेकिन केवल 300-400 साल पहले वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पहले उपकरणों का आविष्कार किया गया था: एक थर्मामीटर, एक मौसम वेन। वर्तमान में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के नेतृत्व में गैस का अध्ययन किया जाता है, जिसमें रूस के अलावा और भी कई शामिल हैं। नवीनतम तकनीकी साधनों का उपयोग करके सामग्री एकत्र करने और प्रसंस्करण के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया गया है। वायुमंडल की स्थिति पर नज़र रखने के लिए, विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित ज़मीन-आधारित मौसम विज्ञान स्टेशनों का एक नेटवर्क बनाया गया है।
तापमान को थर्मामीटर का उपयोग करके मापा जाता है; इसे डिग्री सेल्सियस में मापने की प्रथा है। यह प्रणाली पानी के भौतिक गुणों पर आधारित है: शून्य डिग्री पर यह ठोस अवस्था में बदल जाता है - यह जम जाता है, 100 डिग्री पर - गैसीय अवस्था में। वर्षा की मात्रा वर्षा गेज द्वारा मापी जाती है - दीवारों पर विशेष चिह्नों वाला एक कंटेनर। वायु धाराओं की गति की गति पवन मीटर (एनीमोमीटर) द्वारा मापी जाती है। आमतौर पर इसके बगल में एक मौसम फलक स्थापित किया जाता है, जो हवा की दिशा दर्शाता है। हवाई क्षेत्रों और पुलों के पास जहां खतरा हो सकता है, हवा की दिशा संकेतक स्थापित किए जाते हैं - धारीदार कपड़े से बने बड़े शंकु के आकार के बैग, दोनों तरफ खुले होते हैं। बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है।
मौसम विज्ञान केंद्रों पर दिन में कम से कम 4 बार रीडिंग ली जाती है। स्वचालित रेडियो मौसम विज्ञान स्टेशन दुर्गम क्षेत्रों में संचालित होते हैं। और महासागरों में ऐसे स्टेशन तैरते प्लेटफार्मों पर स्थापित किए जाते हैं। मुक्त वातावरण का अध्ययन रेडियोसॉन्डेस का उपयोग करके किया जाता है - उपकरण जो हाइड्रोजन से भरे मुक्त-उड़ने वाले रबर के गुब्बारों से जुड़े होते हैं। वे 30-40 किमी तक की ऊंचाई पर वायुमंडल की स्थिति पर डेटा एकत्र करते हैं। मौसम संबंधी रॉकेट और भी ऊंचे उठते हैं, 120 किमी तक। एक निश्चित ऊंचाई पर, उपकरणों के साथ रॉकेट का हिस्सा अलग हो जाता है और पैराशूट से पृथ्वी की सतह पर उतारा जाता है। हवा की संरचना को स्पष्ट करने और उच्च ऊंचाई पर स्थित परतों का अध्ययन करने के लिए, रॉकेट का उपयोग किया जाता है जो 500 किमी तक वायुमंडल की जांच करते हैं। वायुमंडल की स्थिति और पृथ्वी की सतह के ऊपर होने वाली मौसम प्रक्रियाओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कृत्रिम पृथ्वी उपग्रहों द्वारा प्रदान की जाती है। अंतरिक्ष में कक्षीय स्टेशनों से अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किए गए वायुमंडलीय घटनाओं के अवलोकन बहुत मूल्यवान हैं।
वीडियो स्रोत: AirPano.ru
वातावरण पर्यावरण प्रदूषण
वायुमंडलीय वायु एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग जीवित जीवों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया में किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न उत्पादन संयंत्रों और इंजनों में किसी भी ईंधन को जलाते समय किया जाता है। वायुमण्डल विमानन द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
प्रकृति में वायु के मुख्य उपभोक्ता पृथ्वी की वनस्पतियाँ और जीव-जंतु हैं। ऐसा अनुमान है कि वायु का संपूर्ण महासागर लगभग दस वर्षों में स्थलीय जीवों से होकर गुजरता है।
वायुमंडल शक्तिशाली सौर विकिरण से व्याप्त है, जो पृथ्वी के थर्मल शासन को नियंत्रित करता है और दुनिया भर में गर्मी के पुनर्वितरण में योगदान देता है। सूर्य से प्राप्त दीप्तिमान ऊर्जा व्यावहारिक रूप से पृथ्वी की सतह के लिए ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यह ऊर्जा वायुमंडल द्वारा आंशिक रूप से अवशोषित होती है। पृथ्वी तक पहुँचने वाली ऊर्जा आंशिक रूप से मिट्टी और पानी द्वारा अवशोषित होती है और आंशिक रूप से उनकी सतह से वायुमंडल में परावर्तित होती है। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी का तापमान शासन कैसा होता: रात में और सर्दियों में यह सौर विकिरण के कारण बहुत ठंडा हो जाता, और गर्मियों में और दिन के दौरान यह अत्यधिक गर्म हो जाता। सौर विकिरण, जैसा कि चंद्रमा पर होता है, जहां कोई वायुमंडल नहीं है।
पृथ्वी पर वायुमंडल के लिए धन्यवाद, ठंढ से गर्मी और वापसी तक कोई तेज संक्रमण नहीं होता है। .
यदि पृथ्वी वायुमंडल से घिरी न होती, तो एक दिन के भीतर तापमान में उतार-चढ़ाव का आयाम 200 C तक पहुंच जाता: दिन के दौरान लगभग +100 C, रात में लगभग 100 C. सर्दियों और गर्मियों के तापमान के बीच और भी अधिक अंतर होता . लेकिन वायुमंडल के कारण, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग +15″C है।
वायुमंडल एक विश्वसनीय ढाल है जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को विनाशकारी पराबैंगनी, एक्स-रे और ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है, जो आंशिक रूप से बिखरी हुई और आंशिक रूप से इसकी ऊपरी परतों में अवशोषित होती हैं।
वायुमंडल पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच पदार्थों का आदान-प्रदान करता है। इसी समय, पृथ्वी सबसे हल्की गैसों - हाइड्रोजन और हीलियम को खो देती है और ब्रह्मांडीय धूल और उल्कापिंड प्राप्त करती है। वातावरण हमें तारे के टुकड़ों से बचाता है। ज्यादातर मामलों में, उल्कापिंड मटर से बड़े नहीं होते; गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, वे 11-64 किमी/सेकंड की जबरदस्त गति से वायुमंडल में टकराते हैं, हवा के साथ घर्षण के कारण वे गर्म हो जाते हैं और ज्यादातर पृथ्वी की सतह से 60-70 किमी की ऊंचाई पर जल जाते हैं। सूर्य से प्राप्त दीप्तिमान ऊर्जा व्यावहारिक रूप से पृथ्वी की सतह के लिए ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यह ऊर्जा वायुमंडल द्वारा आंशिक रूप से अवशोषित होती है। पृथ्वी तक पहुँचने वाली ऊर्जा आंशिक रूप से मिट्टी और पानी द्वारा अवशोषित होती है और आंशिक रूप से उनकी सतह से वायुमंडल में परावर्तित होती है। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी का तापमान शासन कैसा होता: रात में और सर्दियों में यह सौर विकिरण के कारण बहुत ठंडा हो जाता, और गर्मियों में और दिन के दौरान यह अत्यधिक गर्म हो जाता। सौर विकिरण, जैसा कि चंद्रमा पर होता है, जहां कोई वायुमंडल नहीं है।
पृथ्वी पर वायुमंडल के लिए धन्यवाद, ठंढ से गर्मी और वापसी में कोई तेज संक्रमण नहीं होता है। यदि पृथ्वी वायुमंडल से घिरी न होती, तो एक दिन के भीतर तापमान में उतार-चढ़ाव का आयाम 200 C तक पहुंच जाता: दिन के दौरान लगभग +100 C, रात में लगभग 100 C. सर्दियों और गर्मियों के तापमान के बीच और भी अधिक अंतर होता . लेकिन वायुमंडल के कारण, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग +15″C है।
ओजोन स्क्रीन का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक मूल्य है। यह पृथ्वी की सतह से 20-50 किमी की ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन की कुल मात्रा 3.3 बिलियन टन अनुमानित है। इस परत की मोटाई अपेक्षाकृत छोटी है: सामान्य परिस्थितियों में भूमध्य रेखा पर 2 मिमी से ध्रुवों पर 4 मिमी तक। ओजोन स्क्रीन का मुख्य महत्व जीवित जीवों को पराबैंगनी विकिरण से बचाना है।
वायुमंडल एक विश्वसनीय ढाल है जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को विनाशकारी पराबैंगनी, एक्स-रे और ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है, जो आंशिक रूप से बिखरी हुई और आंशिक रूप से इसकी ऊपरी परतों में अवशोषित होती हैं। वायुमंडल पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच पदार्थों का आदान-प्रदान करता है। इसी समय, पृथ्वी सबसे हल्की गैसों - हाइड्रोजन और हीलियम को खो देती है और ब्रह्मांडीय धूल और उल्कापिंड प्राप्त करती है। .
वातावरण हमें तारे के टुकड़ों से बचाता है। ज्यादातर मामलों में, उल्कापिंड मटर से बड़े नहीं होते; गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, वे 11-64 किमी/सेकंड की जबरदस्त गति से वायुमंडल में टकराते हैं, हवा के साथ घर्षण के कारण वे गर्म हो जाते हैं और ज्यादातर पृथ्वी की सतह से 60-70 किमी की ऊंचाई पर जल जाते हैं। प्रकाश के वितरण में वातावरण की बड़ी भूमिका होती है। हवा सूर्य की किरणों को लाखों छोटी-छोटी किरणों में तोड़ती है, उन्हें बिखेरती है और एक समान रोशनी पैदा करती है जिसके हम आदी हैं।
वायु आवरण की उपस्थिति हमारे आकाश को नीला रंग देती है, क्योंकि वायु के मूल तत्वों और उसमें मौजूद विभिन्न अशुद्धियों के अणु मुख्य रूप से छोटी तरंग दैर्ध्य, यानी नीले, नीले, बैंगनी रंग की किरणों को बिखेरते हैं। कभी-कभी वातावरण में अशुद्धियाँ मौजूद होने के कारण आकाश का रंग शुद्ध नहीं होता है। जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं, घनत्व और वायु प्रदूषण कम होता जाता है, यानी। बिखरने वाले कणों की संख्या, आकाश का रंग गहरा हो जाता है, गहरे नीले रंग में बदल जाता है, और समताप मंडल में - काले-बैंगनी में बदल जाता है। वातावरण वह माध्यम है जहाँ ध्वनियाँ यात्रा करती हैं। हवा के बिना, पृथ्वी पर सन्नाटा होगा। हम एक-दूसरे को नहीं सुनेंगे, न ही समुद्र, हवा, जंगल आदि का शोर सुनेंगे। .
आयनमंडल रेडियो संकेतों के प्रसारण और रेडियो तरंगों के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है।
लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि हवा का कोई द्रव्यमान नहीं होता। केवल 17वीं शताब्दी में ही यह सिद्ध हो गया था कि 1 मी 3 शुष्क हवा का द्रव्यमान, यदि समुद्र तल पर 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तौला जाए, तो 1293 ग्राम के बराबर होता है, और पृथ्वी की सतह के प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर के लिए 1033 ग्राम होता है। हवा का जी.
किसी व्यक्ति की हथेली पर लगभग 1471 N के बल के साथ वायु दबाव का अनुभव होता है, और हवा 1471 * 103 N के बल के साथ पूरे मानव शरीर पर दबाव डालती है। हम इस गुरुत्वाकर्षण को केवल इसलिए नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि हमारे शरीर के सभी ऊतक भी हवा से संतृप्त, जो बाहरी दबाव को संतुलित करता है। जब यह संतुलन गड़बड़ा जाता है, तो हमारी भलाई बिगड़ जाती है: नाड़ी तेज हो जाती है, सुस्ती, उदासीनता आदि प्रकट होती है। एक व्यक्ति को पहाड़ पर चढ़ते समय या बड़ी गहराई तक गोता लगाते समय, साथ ही हवाई जहाज से उतरते और उतरते समय समान संवेदनाओं का अनुभव होता है। शीर्ष पर, हवा का दबाव और उसका द्रव्यमान कम हो जाता है: 20 किमी की ऊंचाई पर, 1 मीटर 3 हवा का द्रव्यमान 43 ग्राम है, और 40 किमी की ऊंचाई पर - 4 ग्राम। सूर्य की उज्ज्वल ऊर्जा व्यावहारिक रूप से है पृथ्वी की सतह के लिए ऊष्मा का एकमात्र स्रोत। यह ऊर्जा वायुमंडल द्वारा आंशिक रूप से अवशोषित होती है। पृथ्वी तक पहुँचने वाली ऊर्जा आंशिक रूप से मिट्टी और पानी द्वारा अवशोषित होती है और आंशिक रूप से उनकी सतह से वायुमंडल में परावर्तित होती है। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी का तापमान शासन कैसा होता: रात में और सर्दियों में यह सौर विकिरण के कारण बहुत ठंडा हो जाता, और गर्मियों में और दिन के दौरान यह अत्यधिक गर्म हो जाता। सौर विकिरण, जैसा कि चंद्रमा पर होता है, जहां कोई वायुमंडल नहीं है।
वायुमंडल में विकसित होने वाली सभी प्रक्रियाएँ सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके की जाती हैं। इसके कारण, हर साल पृथ्वी की सतह से अरबों टन पानी वाष्पित हो जाता है। वायुमंडल विश्व पर नमी के पुनर्वितरण के रूप में कार्य करता है।
वायुमंडल के भौतिक गुण और स्थिति बदलती है: 1) समय के साथ - दिन, ऋतुओं, वर्षों के दौरान; 2) अंतरिक्ष में - समुद्र तल से ऊँचाई, क्षेत्र के अक्षांश और समुद्र से दूरी के आधार पर।
वातावरण में हमेशा एक निश्चित मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं। प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में शामिल हैं: धूल (पौधे, ज्वालामुखीय और ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की), धूल भरी आंधी, समुद्री नमक के कण, अपक्षय उत्पाद, कोहरा, जंगल और मैदानी आग से धुआं और गैसें, पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवविज्ञानी मूल के विभिन्न उत्पाद, आदि। प्राकृतिक स्रोत प्रदूषित वातावरण ज्वालामुखी विस्फोट जैसी भयानक प्राकृतिक घटना का प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर यह विनाशकारी होता है. जब ज्वालामुखी फटते हैं, तो भारी मात्रा में गैसें, जलवाष्प, ठोस कण, राख और धूल वायुमंडल में छोड़े जाते हैं; अत्यधिक गर्म पदार्थ हवा में छोड़े जाने से वायुमंडल का तापीय प्रदूषण होता है। .
उनका तापमान इतना होता है कि वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जला देते हैं। ज्वालामुखी गतिविधि के कम होने के बाद, वायुमंडल में गैसों का समग्र संतुलन धीरे-धीरे बहाल हो जाता है।
बड़े जंगल और मैदानी आग वातावरण को काफी प्रदूषित करती हैं। अधिकतर ये शुष्क वर्षों में होते हैं। आग का धुंआ विशाल क्षेत्र में फैल जाता है। तेज हवाओं द्वारा पृथ्वी की सतह से उठे छोटे मिट्टी के कणों के स्थानांतरण के कारण धूल भरी आंधियां आती हैं। तेज़ हवाएँ - बवंडर, तूफ़ान - बड़े चट्टानी टुकड़ों को भी हवा में उठा देती हैं, लेकिन वे अधिक समय तक हवा में नहीं रहते। तेज़ तूफ़ान के दौरान 50 मिलियन टन तक धूल हवा में उठती है। धूल भरी आंधियों का कारण सूखा, गहन जुताई, चराई और जंगलों के विनाश के कारण होने वाली गर्म हवाएँ हैं। मैदानी, अर्ध-रेगिस्तानी और रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियां सबसे आम हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, आग और धूल भरी आंधियों से जुड़ी विनाशकारी घटनाएं पृथ्वी के चारों ओर एक प्रकाश ढाल की उपस्थिति का कारण बनती हैं, जो ग्रह के थर्मल संतुलन को कुछ हद तक बदल देती है। लेकिन अधिकतर ये घटनाएं स्थानीय प्रकृति की होती हैं। अपक्षय और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जुड़ा वायुमंडलीय वायु प्रदूषण बहुत ही मामूली स्थानीय प्रकृति का है। .
प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत या तो वितरित हो सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मांडीय धूल, या अल्पकालिक सहज, उदाहरण के लिए, जंगल और मैदानी आग, ज्वालामुखी विस्फोट, आदि। प्राकृतिक स्रोतों से वायुमंडलीय प्रदूषण का स्तर पृष्ठभूमि है और समय के साथ थोड़ा बदलता है। कृत्रिम प्रदूषण वातावरण के लिए सबसे खतरनाक है। प्रदूषकों की उच्च सांद्रता वाले सबसे स्थिर क्षेत्र सक्रिय मानव गतिविधि के स्थानों में होते हैं। मानवजनित प्रदूषण की विशेषता विभिन्न प्रकार और असंख्य स्रोत हैं। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी विस्फोट जैसी भयानक प्राकृतिक घटनाएँ हैं। आमतौर पर यह विनाशकारी होता है. जब ज्वालामुखी फटते हैं, तो भारी मात्रा में गैसें, जलवाष्प, ठोस कण, राख और धूल वायुमंडल में छोड़े जाते हैं; अत्यधिक गर्म पदार्थ हवा में छोड़े जाने से वायुमंडल का तापीय प्रदूषण होता है। उनका तापमान इतना होता है कि वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जला देते हैं। ज्वालामुखी गतिविधि के कम होने के बाद, वायुमंडल में गैसों का समग्र संतुलन धीरे-धीरे बहाल हो जाता है। .
वायु प्रदूषण की समस्या कोई नयी नहीं है. दो शताब्दियों से भी पहले, कई यूरोपीय देशों में बड़े औद्योगिक केंद्रों में वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। हालाँकि, लंबे समय तक ये प्रदूषण स्थानीय प्रकृति के थे। धुएं और कालिख ने वायुमंडल के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों को प्रदूषित कर दिया और आसानी से स्वच्छ हवा के द्रव्यमान में घुल गए, उस समय जब कुछ कारखाने थे और रासायनिक तत्वों का उपयोग सीमित था। यदि 20वीं सदी की शुरुआत में। उद्योग में 19 रासायनिक तत्वों का उपयोग किया गया था; सदी के मध्य में, लगभग 50 तत्वों का उपयोग पहले ही किया जा चुका था; वर्तमान में, आवर्त सारणी के लगभग सभी तत्वों का उपयोग किया गया था। इसने औद्योगिक उत्सर्जन की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और भारी और दुर्लभ धातुओं, सिंथेटिक यौगिकों, गैर-मौजूद और गैर-प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी, कार्सिनोजेनिक, बैक्टीरियोलॉजिकल और अन्य पदार्थों के एरोसोल के साथ गुणात्मक रूप से नए वायुमंडलीय प्रदूषण को जन्म दिया।
उद्योग और परिवहन की तीव्र वृद्धि का मतलब है कि इतनी मात्रा में उत्सर्जन अब नष्ट नहीं किया जा सकता है। उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके जीवमंडल के लिए खतरनाक और घातक परिणाम भी होते हैं। यह समस्या विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति की अवधि के दौरान, औद्योगिक उत्पादन, बिजली के उत्पादन और खपत, बड़ी संख्या में बिजली के उत्पादन और उपयोग की अत्यधिक उच्च विकास दर की विशेषता के कारण तीव्र हो गई। वाहन.
मुख्य वायु प्रदूषण कई उद्योगों, मोटर परिवहन और गर्मी और बिजली उत्पादन द्वारा उत्पन्न होता है। इसके अलावा, वायु प्रदूषण में उनकी भागीदारी निम्नानुसार वितरित की जाती है: लौह और अलौह धातु विज्ञान, तेल उत्पादन, पेट्रोकेमिस्ट्री, निर्माण सामग्री का उत्पादन, रासायनिक उद्योग - 30%; थर्मल पावर इंजीनियरिंग - 30, मोटर परिवहन - 40%।
वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले सबसे आम जहरीले पदार्थ हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO 2, कार्बन डाइऑक्साइड CO 2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO x, हाइड्रोकार्बन C p N m और धूल। बड़े औद्योगिक शहरों के वातावरण में हानिकारक पदार्थों की अनुमानित सापेक्ष संरचना है: CO - 45%, SO - 18%, CH - 15%, धूल - 12%। .
इन पदार्थों के अलावा, अन्य अधिक विषैले पदार्थ भी प्रदूषित वायुमंडलीय वायु में पाए जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कारखानों से निकलने वाले वेंटिलेशन उत्सर्जन में हाइड्रोफ्लोरिक, सल्फ्यूरिक, क्रोमिक और अन्य खनिज एसिड, कार्बनिक सॉल्वैंट्स आदि के वाष्प होते हैं। वर्तमान में, 500 से अधिक हानिकारक पदार्थ हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, और उनकी संख्या बढ़ रही है। कृत्रिम प्रदूषण वातावरण के लिए सबसे खतरनाक है। प्रदूषकों की उच्च सांद्रता वाले सबसे स्थिर क्षेत्र सक्रिय मानव गतिविधि के स्थानों में होते हैं। मानवजनित प्रदूषण की विशेषता विभिन्न प्रकार और असंख्य स्रोत हैं। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी विस्फोट जैसी भयानक प्राकृतिक घटनाएँ हैं। आमतौर पर यह विनाशकारी होता है. जब ज्वालामुखी फटते हैं, तो भारी मात्रा में गैसें, जलवाष्प, ठोस कण, राख और धूल वायुमंडल में छोड़े जाते हैं; अत्यधिक गर्म पदार्थ हवा में छोड़े जाने से वायुमंडल का तापीय प्रदूषण होता है। उनका तापमान इतना होता है कि वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जला देते हैं। ज्वालामुखी गतिविधि के कम होने के बाद, वायुमंडल में गैसों का समग्र संतुलन धीरे-धीरे बहाल हो जाता है।
पृथ्वी के जीवन में वायुमंडल की भूमिका
वायुमंडल पृथ्वी ग्रह के चारों ओर एक गैसीय आवरण है। इसकी आंतरिक सतह जलमंडल और आंशिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी को कवर करती है, जबकि इसकी बाहरी सतह बाहरी अंतरिक्ष के पृथ्वी के निकट भाग की सीमा बनाती है।
वायुमंडल का अध्ययन करने वाली भौतिकी और रसायन विज्ञान की शाखाओं के समूह को आमतौर पर वायुमंडलीय भौतिकी कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर मौसम का निर्धारण करता है, मौसम विज्ञान मौसम का अध्ययन करता है, और जलवायु विज्ञान दीर्घकालिक जलवायु विविधताओं से संबंधित है।
पहले से ही समुद्र तल से 5 किमी की ऊंचाई पर, एक अप्रशिक्षित व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी का अनुभव होने लगता है और अनुकूलन के बिना, एक व्यक्ति का प्रदर्शन काफी कम हो जाता है। वायुमंडल का शारीरिक क्षेत्र यहीं समाप्त होता है। 9 किमी की ऊंचाई पर मानव का सांस लेना असंभव हो जाता है, हालांकि लगभग 115 किमी तक वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है।
वातावरण हमें साँस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। हालाँकि, वायुमंडल के कुल दबाव में गिरावट के कारण, जैसे-जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते हैं, ऑक्सीजन का आंशिक दबाव तदनुसार कम हो जाता है।
मानव फेफड़ों में लगातार लगभग 3 लीटर वायुकोशीय वायु होती है। सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर वायुकोशीय वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव 110 mmHg होता है। कला।, कार्बन डाइऑक्साइड दबाव - 40 मिमी एचजी। कला।, और जल वाष्प - 47 मिमी एचजी। कला। बढ़ती ऊंचाई के साथ, ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है, और फेफड़ों में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का कुल वाष्प दबाव लगभग स्थिर रहता है - लगभग 87 मिमी एचजी। कला। जब परिवेशी वायु का दबाव इस मान के बराबर हो जाएगा तो फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो जाएगी।
लगभग 19-20 किमी की ऊंचाई पर, वायुमंडलीय दबाव 47 मिमी एचजी तक गिर जाता है। कला। इसलिए, इस ऊंचाई पर, मानव शरीर में पानी और अंतरालीय द्रव उबलने लगते हैं। इन ऊंचाइयों पर दबाव वाले केबिन के बाहर, मृत्यु लगभग तुरंत हो जाती है। इस प्रकार, मानव शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से, "अंतरिक्ष" पहले से ही 15-19 किमी की ऊंचाई पर शुरू होता है।
हवा की घनी परतें - क्षोभमंडल और समतापमंडल - हमें विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाती हैं। हवा के पर्याप्त विरलीकरण के साथ, 36 किमी से अधिक की ऊंचाई पर, आयनकारी विकिरण - प्राथमिक ब्रह्मांडीय किरणें - का शरीर पर तीव्र प्रभाव पड़ता है; 40 किमी से अधिक की ऊंचाई पर, सौर स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी भाग मनुष्यों के लिए खतरनाक है। वायुमंडल ऑक्सीजन समताप मंडल विकिरण
जैसे-जैसे हम पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वायुमंडल की निचली परतों में ध्वनि प्रसार, वायुगतिकीय लिफ्ट और ड्रैग की घटना, संवहन द्वारा गर्मी हस्तांतरण आदि जैसी परिचित घटनाएं धीरे-धीरे कमजोर हो जाती हैं और फिर पूरी तरह से गायब हो जाती हैं।
वायु की विरल परतों में ध्वनि का प्रसार असंभव है। 60-90 किमी की ऊंचाई तक, नियंत्रित वायुगतिकीय उड़ान के लिए वायु प्रतिरोध और लिफ्ट का उपयोग करना अभी भी संभव है।
लेकिन 100-130 किमी की ऊंचाई से शुरू होकर, एम संख्या और ध्वनि अवरोध की अवधारणाएं, जो हर पायलट से परिचित हैं, अपना अर्थ खो देती हैं: पारंपरिक कर्मन रेखा निहित है, जिसके आगे विशुद्ध रूप से बैलिस्टिक उड़ान का क्षेत्र शुरू होता है, जो केवल हो सकता है प्रतिक्रियाशील बलों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाए।
100 किमी से ऊपर की ऊंचाई पर, वायुमंडल एक और उल्लेखनीय संपत्ति से वंचित है - संवहन द्वारा थर्मल ऊर्जा को अवशोषित करने, संचालित करने और संचारित करने की क्षमता (यानी हवा को मिलाकर)। इसका मतलब यह है कि कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उपकरणों के विभिन्न तत्वों को बाहर से उसी तरह से ठंडा नहीं किया जा सकेगा जैसा आमतौर पर हवाई जहाज पर किया जाता है - एयर जेट और एयर रेडिएटर्स की मदद से। इस ऊंचाई पर, जैसा कि आम तौर पर अंतरिक्ष में होता है, गर्मी स्थानांतरित करने का एकमात्र तरीका थर्मल विकिरण है।
हमारे चारों ओर की दुनिया तीन अलग-अलग हिस्सों से बनी है: पृथ्वी, जल और वायु। उनमें से प्रत्येक अपने तरीके से अद्वितीय और दिलचस्प है। अब हम उनमें से केवल अंतिम के बारे में बात करेंगे। वातावरण क्या है? यह कैसे घटित हुआ? इसमें क्या शामिल है और इसे किन भागों में विभाजित किया गया है? ये सभी सवाल बेहद दिलचस्प हैं.
"वातावरण" नाम स्वयं ग्रीक मूल के दो शब्दों से बना है, रूसी में अनुवादित उनका अर्थ है "भाप" और "गेंद"। और यदि आप सटीक परिभाषा को देखें, तो आप निम्नलिखित पढ़ सकते हैं: "वायुमंडल पृथ्वी ग्रह का वायु कवच है, जो बाहरी अंतरिक्ष में इसके साथ-साथ चलता है।" इसका विकास ग्रह पर होने वाली भूवैज्ञानिक और भू-रासायनिक प्रक्रियाओं के समानांतर हुआ। और आज जीवित जीवों में होने वाली सभी प्रक्रियाएँ इसी पर निर्भर हैं। वायुमंडल के बिना, ग्रह चंद्रमा की तरह एक निर्जीव रेगिस्तान बन जाएगा।
इसमें क्या शामिल होता है?
वातावरण क्या है और इसमें कौन से तत्व शामिल हैं, इस सवाल में लंबे समय से लोगों की दिलचस्पी रही है। इस खोल के मुख्य घटक 1774 में पहले से ही ज्ञात थे। इन्हें एंटोनी लवॉज़ियर द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने पाया कि वायुमंडल की संरचना मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। समय के साथ, इसके घटकों को परिष्कृत किया गया। और अब पता चला है कि इसमें पानी और धूल के अलावा कई अन्य गैसें भी शामिल हैं।
आइए इस पर करीब से नज़र डालें कि पृथ्वी की सतह के निकट उसका वायुमंडल किससे बनता है। सबसे आम गैस नाइट्रोजन है। इसमें 78 प्रतिशत से थोड़ा अधिक होता है। लेकिन, इतनी बड़ी मात्रा के बावजूद, नाइट्रोजन हवा में व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय है।

मात्रा की दृष्टि से अगला और महत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व ऑक्सीजन है। इस गैस में लगभग 21% होता है, और यह बहुत उच्च गतिविधि प्रदर्शित करता है। इसका विशिष्ट कार्य मृत कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करना है, जो इस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप विघटित हो जाते हैं।
कम लेकिन महत्वपूर्ण गैसें
तीसरी गैस जो वायुमंडल का हिस्सा है वह आर्गन है। यह एक प्रतिशत से थोड़ा कम है. इसके बाद नियॉन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के साथ हीलियम, हाइड्रोजन के साथ क्रिप्टन, क्सीनन, ओजोन और यहां तक कि अमोनिया भी आता है। लेकिन उनमें से इतने कम हैं कि ऐसे घटकों का प्रतिशत सौवें, हज़ारवें और मिलियनवें के बराबर है। इनमें से, केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह वह निर्माण सामग्री है जिसकी पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। इसका अन्य महत्वपूर्ण कार्य विकिरण को रोकना और सूर्य की कुछ गर्मी को अवशोषित करना है।

एक अन्य छोटी लेकिन महत्वपूर्ण गैस, ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोकने के लिए मौजूद है। इस संपत्ति के लिए धन्यवाद, ग्रह पर सारा जीवन विश्वसनीय रूप से संरक्षित है। दूसरी ओर, ओजोन समताप मंडल के तापमान को प्रभावित करता है। इस तथ्य के कारण कि यह इस विकिरण को अवशोषित करता है, हवा गर्म हो जाती है।
बिना रुके मिश्रण द्वारा वायुमंडल की मात्रात्मक संरचना की स्थिरता बनाए रखी जाती है। इसकी परतें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से चलती हैं। इसलिए, विश्व में कहीं भी पर्याप्त ऑक्सीजन है और अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है।
हवा में और क्या है?
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हवाई क्षेत्र में भाप और धूल पाई जा सकती है। उत्तरार्द्ध में पराग और मिट्टी के कण होते हैं; शहर में वे निकास गैसों से ठोस उत्सर्जन की अशुद्धियों से जुड़ जाते हैं।
लेकिन वातावरण में पानी बहुत है. कुछ शर्तों के तहत, यह संघनित होता है और बादल और कोहरा दिखाई देता है। संक्षेप में, ये एक ही चीज़ हैं, केवल पहला पृथ्वी की सतह से ऊपर दिखाई देता है, और आखिरी वाला इसके साथ फैलता है। बादल अलग-अलग आकार लेते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करती है।
यदि वे भूमि से 2 किमी ऊपर बने हों, तो उन्हें परतदार कहा जाता है। उन्हीं से ज़मीन पर बारिश होती है या बर्फ़ गिरती है। इनके ऊपर 8 किमी की ऊंचाई तक क्यूम्यलस बादल बनते हैं। वे हमेशा सबसे सुंदर और सुरम्य होते हैं। वे ही हैं जो उन्हें देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि वे कैसे दिखते हैं। यदि ऐसी संरचनाएं अगले 10 किमी में दिखाई देती हैं, तो वे बहुत हल्की और हवादार होंगी। इनका नाम पंखदार है.

वायुमंडल को किन परतों में विभाजित किया गया है?
यद्यपि उनका तापमान एक-दूसरे से बहुत भिन्न होता है, यह बताना बहुत मुश्किल है कि एक परत किस विशिष्ट ऊंचाई पर शुरू होती है और दूसरी किस ऊंचाई पर समाप्त होती है। यह विभाजन बहुत सशर्त और अनुमानित है। हालाँकि, वायुमंडल की परतें अभी भी मौजूद हैं और अपना कार्य करती हैं।
वायुमण्डल का सबसे निचला भाग क्षोभमण्डल कहलाता है। जैसे-जैसे यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर 8 से 18 किमी तक बढ़ता है, इसकी मोटाई बढ़ती जाती है। यह वायुमंडल का सबसे गर्म भाग है क्योंकि इसमें हवा पृथ्वी की सतह से गर्म होती है। अधिकांश जलवाष्प क्षोभमंडल में केंद्रित है, जिसके कारण बादल बनते हैं, वर्षा होती है, गरज के साथ गड़गड़ाहट होती है और हवाएँ चलती हैं।
अगली परत लगभग 40 किमी मोटी है और इसे समताप मंडल कहा जाता है। यदि कोई पर्यवेक्षक हवा के इस हिस्से में जाता है, तो वह पाएगा कि आकाश बैंगनी हो गया है। यह पदार्थ के कम घनत्व द्वारा समझाया गया है, जो व्यावहारिक रूप से सूर्य की किरणों को बिखेरता नहीं है। इसी परत में जेट विमान उड़ान भरते हैं। सभी खुले स्थान उनके लिए खुले हैं, क्योंकि व्यावहारिक रूप से कोई बादल नहीं हैं। समताप मंडल के अंदर एक परत होती है जिसमें बड़ी मात्रा में ओजोन होती है।

इसके बाद स्ट्रेटोपॉज़ और मेसोस्फीयर आते हैं। उत्तरार्द्ध लगभग 30 किमी मोटा है। यह वायु घनत्व और तापमान में तीव्र कमी की विशेषता है। प्रेक्षक को आकाश काला दिखाई देता है। यहां आप दिन में तारे भी देख सकते हैं।
परतें जिनमें व्यावहारिक रूप से कोई हवा नहीं होती है
वायुमंडल की संरचना थर्मोस्फीयर नामक एक परत के साथ जारी रहती है - अन्य सभी की तुलना में सबसे लंबी, इसकी मोटाई 400 किमी तक पहुंचती है। यह परत अपने विशाल तापमान से अलग है, जो 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
अंतिम दो क्षेत्रों को अक्सर एक में जोड़ दिया जाता है और आयनमंडल कहा जाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि आयनों की रिहाई के साथ उनमें प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये परतें ही हैं जो उत्तरी रोशनी जैसी प्राकृतिक घटना का निरीक्षण करना संभव बनाती हैं।

पृथ्वी से अगला 50 किमी बाह्यमंडल को आवंटित किया गया है। यह वायुमंडल का बाहरी आवरण है। यह वायु के कणों को अंतरिक्ष में फैला देता है। मौसम उपग्रह आमतौर पर इसी परत में घूमते हैं।
पृथ्वी का वायुमंडल मैग्नेटोस्फीयर के साथ समाप्त होता है। यह वह है जिसने ग्रह के अधिकांश कृत्रिम उपग्रहों को आश्रय दिया है।
इतना सब कुछ कहने के बाद माहौल क्या है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। यदि आपको इसकी आवश्यकता के बारे में संदेह है, तो उन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है।
वातावरण का अर्थ
वायुमंडल का मुख्य कार्य ग्रह की सतह को दिन के दौरान अत्यधिक गर्म होने और रात में अत्यधिक ठंडक से बचाना है। इस शेल का अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य, जिस पर कोई विवाद नहीं करेगा, सभी जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना है। इसके बिना उनका दम घुट जाएगा.
अधिकांश उल्कापिंड ऊपरी परतों में ही जल जाते हैं, पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं पहुंच पाते। और लोग उड़ती रोशनी को टूटते तारे समझकर प्रशंसा कर सकते हैं। वायुमंडल के बिना, पूरी पृथ्वी गड्ढों से अटी पड़ी होगी। और सौर विकिरण से सुरक्षा पर पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है।
कोई व्यक्ति वातावरण को कैसे प्रभावित करता है?
बहुत नकारात्मक. इसका कारण लोगों की बढ़ती सक्रियता है। सभी नकारात्मक पहलुओं का मुख्य हिस्सा उद्योग और परिवहन पर पड़ता है। वैसे, यह कारें ही हैं जो वायुमंडल में प्रवेश करने वाले सभी प्रदूषकों का लगभग 60% उत्सर्जित करती हैं। शेष चालीस ऊर्जा और उद्योग, साथ ही अपशिष्ट निपटान उद्योगों के बीच विभाजित हैं।

प्रतिदिन वायु की पूर्ति करने वाले हानिकारक पदार्थों की सूची बहुत लंबी है। वातावरण में परिवहन के कारण हैं: नाइट्रोजन और सल्फर, कार्बन, नीला और कालिख, साथ ही एक मजबूत कार्सिनोजेन जो त्वचा कैंसर का कारण बनता है - बेंज़ोपाइरीन।
उद्योग में निम्नलिखित रासायनिक तत्व शामिल हैं: सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और फिनोल, क्लोरीन और फ्लोरीन। यदि प्रक्रिया जारी रही, तो जल्द ही सवालों के जवाब मिलेंगे: “माहौल कैसा है? इसमें क्या शामिल होता है? बिल्कुल अलग होगा.
6.2. वायुमंडल का अर्थ एवं संरचना
यदि पानी, जिसकी लंबे समय से कमी थी, को "जीवन का संसाधन" कहा जाता था, तो हवा को केवल हमारे शहरीकृत युग में ही याद किया जाता था। आइए याद रखें कि एक व्यक्ति भोजन के बिना कई दसियों दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन हवा के बिना - केवल 5-7 मिनट तक। इसके अलावा, लोगों को स्वच्छ हवा की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति, विशेष रूप से शहरों और औद्योगिक केंद्रों में, कम है।
वातावरण का अर्थ. वायुमंडलीय वायु सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है गंतव्य (पृथ्वी और मानवता के लिए ):
लोगों, वनस्पतियों और जीवों को महत्वपूर्ण गैस तत्व (ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड) प्रदान करें;
तापमान परिवर्तन को कम करें (हवा गर्मी और ठंड का खराब संवाहक है), यानी। ग्रह पर थर्मोरेग्यूलेशन सुनिश्चित करें;
पृथ्वी की सतह को ब्रह्मांडीय, विकिरण और पराबैंगनी सौर विकिरण से सुरक्षित रखें;
पृथ्वी को उल्कापिंडों और अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों से बचाएं, जिनका भारी द्रव्यमान वायुमंडल में जल जाता है;
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तटस्थ गैसों के साथ औद्योगिक मानवजनित प्रक्रियाएं प्रदान करें।
वायुमंडल पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित गर्मी को अंतरिक्ष में अवशोषित करके और इसे आंशिक रूप से काउंटर विकिरण के रूप में वापस करके हमारे ग्रह को "गर्म" करता है। वायुमंडल सूर्य की किरणों को बिखेरता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश से छाया (गोधूलि) में क्रमिक संक्रमण होता है। रात में, यह प्रकाश किरणें उत्सर्जित करता है और पृथ्वी की सतह पर रोशनी के स्रोत के रूप में कार्य करता है।
वायुमंडल की रात्रि चमक (ल्यूमिनसेंस) 80 से 300 किमी की ऊंचाई पर दुर्लभ वायु गैसों की चमक है। यह चांदनी रात में पृथ्वी की सतह की कुल रोशनी का 40-45% प्रदान करता है, जबकि तारों का प्रकाश लगभग 30% होता है, और अंतरतारकीय धूल द्वारा बिखरा हुआ प्रकाश शेष 25-30% होता है। ऑरोरा बोरेलिस एक प्रकार की वायुमंडलीय चमक है। पृथ्वी पर, वे बादलों की अनुपस्थिति में केवल रात में उच्च अक्षांशों पर देखे जाते हैं। अंतरिक्ष से, अरोरा हमेशा दिखाई देते हैं, और साथ ही बड़े क्षेत्रों में भी।
वातावरण की संरचना. वायुमंडल में कई परतें होती हैं - गोले, जिनके बीच कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएँ नहीं होती हैं।
1. क्षोभमण्डल - वायुमंडल की निचली मुख्य परत। यह सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवों से 10 किमी ऊपर, समशीतोष्ण अक्षांशों में 12 किमी और भूमध्य रेखा से 18 किमी ऊपर तक पहुंचती है।
क्षोभमंडल में वायुमंडलीय वायु के कुल द्रव्यमान का 4/5 से अधिक भाग होता है। विभिन्न मौसम संबंधी घटनाएं इसमें सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। ह ज्ञात है कि 1 किमी की वृद्धि के साथ, इस परत में हवा का तापमान 6 डिग्री से अधिक कम हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा सूर्य की किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने देती है, जो इसे गर्म कर देती है। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी से सटी वायुमंडल की परतें भी गर्म हो जाती हैं।
सर्दियों में, पृथ्वी की सतह बहुत ठंडी हो जाती है, जो बर्फ के आवरण से सुगम होती है, जो सूर्य की अधिकांश किरणों को परावर्तित करती है। इस कारण से, पृथ्वी की सतह पर हवा शीर्ष की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है, अर्थात तथाकथित तापमान व्युत्क्रमण.रात में अक्सर तापमान में उलटफेर देखा जाता है।
गर्मियों में, पृथ्वी की सतह सूर्य की किरणों से अत्यधिक और असमान रूप से गर्म होती है। इसके सर्वाधिक गर्म क्षेत्रों से हवा के भंवर ऊपर की ओर उठते हैं। ऊपर उठने वाली हवा का स्थान पृथ्वी के कम गर्म क्षेत्रों से आने वाली हवा ले लेती है, जिसके बदले में वायुमंडल की ऊपरी परतों से आने वाली हवा ले लेती है। उमड़ती संवहन,जिससे वायुमंडल ऊर्ध्वाधर दिशा में मिश्रित हो जाता है। संवहन कोहरे को खत्म करने में मदद करता है और वायुमंडल की निचली परत में धूल को कम करता है।
12-17 किमी की ऊंचाई पर क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में, जब विमान उड़ते हैं, तो अक्सर सफेद बादलों के निशान बनते हैं, जो काफी दूरी से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इन निशानों को कहा जाता है वाष्पीकरण, या निशान व्युत्क्रम।संघनन ट्रेल्स का मुख्य कारण विमान के इंजनों की निकास गैसों के साथ वायुमंडल में प्रवेश करने वाले जल वाष्प का संघनन या उर्ध्वपातन है, क्योंकि जब विमान के इंजन में मिट्टी का तेल जलाया जाता है, तो जल वाष्प बनता है।
एक इंजन में 1 किलोग्राम ईंधन जलाने के लिए लगभग 11 किलोग्राम वायुमंडलीय वायु की खपत होती है, जिससे लगभग 12 किलोग्राम निकास गैसें उत्पन्न होती हैं जिनमें लगभग 1.4 किलोग्राम जल वाष्प होता है।
2. समतापमंडल क्षोभमंडल के ऊपर 50-55 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें समस्त वायुमंडलीय वायु के द्रव्यमान का 20% से कम होता है। इस परत में गैसों की हल्की गति होती है और तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है (ऊपरी सीमा पर 0 0 C तक)।
समताप मंडल का निचला भाग एक मोटी धारणीय परत है जिसके नीचे जलवाष्प, बर्फ के क्रिस्टल और अन्य ठोस कण जमा होते हैं। यहां सापेक्षिक आर्द्रता सदैव 100% के करीब रहती है।
समताप मंडल मेंस्थित ओज़ोन की परत,जीवन-विनाशकारी ब्रह्मांडीय विकिरण और आंशिक रूप से सूर्य की पराबैंगनी किरणों को प्रतिबिंबित करता है। उच्चतम सांद्रता ओजोन 15-35 किमी की ऊंचाई पर मौजूद है, जहां सौर विकिरण के प्रभाव में मुक्त ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है .
3. मेसोस्फीयर समताप मंडल के ऊपर लगभग 50 से 80 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह हवा का 1% से भी कम हिस्सा है। इसकी विशेषता बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, समताप मंडल की सीमा पर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर मेसोस्फीयर की ऊपरी परतों में -90 डिग्री सेल्सियस तक की कमी है।
4. योण क्षेत्र मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित है। यह वायुमंडलीय आयनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक महत्वपूर्ण सामग्री की विशेषता है। आयनमंडल में, पराबैंगनी और एक्स-रे सौर विकिरण के प्रभाव में, अत्यधिक दुर्लभ हवा का आयनीकरण, साथ ही ब्रह्मांडीय विकिरण होता है, जो वायुमंडलीय गैस अणुओं के आयनों और इलेक्ट्रॉनों में अपघटन का कारण बनता है। 80 से 400 किमी की ऊंचाई पर आयनीकरण विशेष रूप से तीव्र होता है। आयनमंडल रेडियो तरंगों के प्रसार को सुगम बनाता है। आयनमंडल की ऊपरी सीमा पृथ्वी के चुंबकमंडल का बाहरी भाग है। आयनमंडल को अक्सर आयनमंडल कहा जाता है बाह्य वायुमंडल.